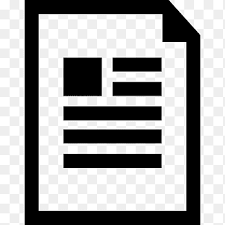भागवत का भाषण और आरएसएस विचारधारा: एक करीबी नजर
– कविता कृष्णन
पिछले साल की शुरूआत में आरएसएस के राष्ट्रीय सम्मेलन में मोहन भागवत के भाषण दोहरी-जुबान बोलने के ही थोड़े जटिल प्रयास थे, जिसमें उन्होंने संघी विचारधारा के तत्वों पर ‘उदार’ रंग चढ़ाने की कोशिश की थी.
करीब से देखें, तो भागवत संघी विचारधारा से तनिक भी नहीं हिले हैं. यह तो भारतीय मीडिया (अथवा इसका अधिकांश हिस्सा) है जो उनके भाषणों को ठीक से जांच-परख का अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर सका और आलोचनात्मक ढंग से देखने के बजाय उनके जुमलों को बस, यूं ही दुहराता रहा.
जाति-आधारित कोटा का विरोध
मसलन, खबरों के अनुसार भागवत ने कहा कि समाज को जाति व्यवस्था के बगैर आगे बढ़ने की जरूरत है, और फिर कहा कि “आरक्षण जारी रहे या न रहे यह फैसला उनको करना है, जिन्हें आरक्षण दिया गया है.” यह वक्तव्य चेतावनी की घंटी है: जिस प्रकार मोदी सरकार आज लोगों को सब्सिडी छोड़ देने को कह रहे हैं, क्या उसी तर्ज पर आरएसएस एससी/एसटी और ओबीसी श्रेणियों पर आरक्षण छोड़ने का दबाव बनाना शुरू करेगा ? (भागवत का वक्तव्य हैवेल्स पंखा के लिए 2016 के एक टीवी प्रचार की याद दिलाता है. ‘हवा बदलेगी’ के नारे के साथ उस प्रचार में दिखाया गया कि एक नवयुवती अपने पिता द्वारा लाए गए एक फाॅर्म को भरने से इनकार कर रही है जिसपर “कोटा” शब्द लिखा हुआ था, जिसका आशय था अधिक “मेरिट वाले” और नैतिक रूप से अधिक योग्य लोगों के लिए आरक्षण छोड़ देना. जब इसका प्रतिवाद हुआ, तो हैवेल्स को यह प्रचार वापस लेना पड़ा. लेकिन भागवत के वक्तव्य का आशय है कि आरएसएस अपनी परंपरागत आरक्षण-विरोधी कट्टरता को काॅरपोरेट-प्रायोजित आरक्षण-विरोधी प्रचार के साथ मिलाने की कोशिश कर सकता है, जिसमें आरक्षण के लाभार्थियों को लानतें भेजी जाती हैं, ताकि वे इसे छोड़ दें.)
अपने इस वक्तव्य के बाद भागवत यह कहते हुए जाति-भेद की निरंतरता के लिए जाति-आधारित आरक्षण पर आरोप लगाते हैं कि “जबतक कोटा और आरक्षण रहेगा, तब तक हम जातियों में बंटे रहेंगे.” 2015 में भी बिहार विधान सभा चुनाव के ठीक पहले भागवत ने जाति-आधारित आरक्षण का विरोध किया था.
जाति-विभेद के लिए ब्राह्मणवाद के बजाए जाति-आधारित आरक्षण को कोसने का मतलब बिलकुल स्पष्ट है. अपने ‘बंच ऑफ थाॅट्स’ (सर्वप्रथम 1966 में प्रकाशित, फिर साहित्य सिंधु प्रकाशन द्वारा 2000 में पुनप्रकाशित) में आरएसएस गुरू गोलवरकर ने लिखा है कि जाति-आधारित आरक्षण की मांग करना या इसे जारी रखना “विभाजनकारी बातें” हैं, और उन्होंने जोर देकर कहा, “हमें जाति, नस्ल आदि के आधार पर समूह बनाने और सेवाओं, वित्तीय मदद, शैक्षिक संस्थाओं और ऐसे अन्य क्षेत्रों में भर्ती आदि विशेषाधिकारों की मांग करने को रोकने के लिए आवाज बुलंद करनी चाहिए. “अल्पसंख्यकों” और “समुदायों” के अर्थ में चर्चा और चिंतन को पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए.” आरएसएस के विश्व-दृष्टिकोण में शांति और ‘समरसता’ तभी कायम की जा सकती है, जब सामाजिक श्रेणी-विभाजन को कोई चुनौती नहीं दी जाए. अगर दलित या पिछड़ी जातियां अथवा महिलाएं जातीय व लैंगिक श्रेणी-विभाजन को चुनौती देती हैं, तो उन्हें ही विभाजनकारी माना जाएगा: ये ब्राह्मणवादी कुलाधीश इन श्रेणी-विभाजनों के अस्तित्व को नकारने भर से खुद को ‘राष्ट्रवादी’ घोषित कर दे सकते हैं और ‘एकता’ को बुलंद करने का दावा ठोंक सकते हैं.
प्रतिगामी पितृसत्तात्मक विचार
इसी प्रकार, कुछ अपवादों को छोड़कर मुख्यधारा मीडिया ने बड़े अदब से रिपोर्ट की है कि भागवत भारतीय समाज को समय के अनुसार आगे बढ़ता देखना चाहते हैं, और कि उन्होंने समलैंगिकता जैसी चीजों तथा किन्नर आदि समूहों को भी स्वीकार किया है. दरअसल, समलैंगिकता के बारे में सवाल का जवाब देते हुए भागवत ने यह अस्पष्ट पंक्ति भी कही कि “समाज के स्वास्थ्य पर भी” ध्यान देना चाहिए. इसमें निहित समलैंगिकता के प्रति घोर नफरत बिलकुल स्पष्ट है: भागवत मानते हैं कि समलैंगिकता समाज के लिए “स्वास्थ्यकर” नहीं है.
जब महिलाओं के अधिकार की बात आई तो भागवत आरएसएस के संस्थापक हेडगेवार के प्रतिगामी तर्कों से रत्ती भर भी नहीं हटे. यह पूछने पर कि आरएसएस में महिलाएं क्यों नहीं हैं, उन्होंने 1931 में एक महिला द्वारा पूछे गए ऐसे ही एक सवाल में हेडगेवार के जवाब को उद्धृत कर दिया, “हेडगेवार ने कहा है कि यह समाज ऐसा नहीं है जहां पुरुष महिलाओं के साथ मिलकर काम कर सकें. इससे अफवाह फैलने की गुंजाइश बन जाएगी.” बात तो यह है कि हेडगेवार के विचार न सिर्फ 21वीं सदी के भारत के लिए, बल्कि 1931 के उस अतीत में भी प्रतिक्रियावादी और प्रतिगामी थे. 1920-दशक से ही, भारतीय महिलाएं न सिर्फ कारखानों में पुरुषों के साथ मिलकर काम करने लगी थीं, बल्कि वे भारत की आजादी के लिए लड़ने वाले विभिन्न राजनीतिक ग्रुपों में भी सक्रियता से शामिल थीं, यहां तक कि 1857 में भी लक्ष्मी बाई, हजरत महल, झलकारी बाई, उदा देवी और अजीजन बाई ने पुरुषों के साथ मिलकर अंगरेजों से लड़ाइयां की थीं. 1931 में कल्पना दत्ता इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की चटगांव शाखा में शामिल हुई थीं – यह सूर्य सेन की अगुवाई में बना एक हथियारबंद प्रतिरोध ग्रुप था, और प्रीतिलता वाडेदर भी इसी ग्रुप में शामिल होकर 1932 में शहीद हुई थीं. दुर्गावती देवी (दुर्गा भाभी) 1928 में भगत सिंह के नेतृत्व में गठित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी (एसएसआरए) की एक सक्रिय सदस्य थीं. भारत की हजारों महिलाएं ‘दांडी मार्च’ और 1930 के नागरिक अवज्ञा आंदोलन में पुरुषों के साथ-साथ शिरकत कर रही थीं. यह विचार अत्यंत प्रतिगामी है कि महिलाओं को अपने कार्यस्थलों पर और साथ ही साथ राजनीतिक संगठनों में यौनिक / नैतिक चरित्र के बारे में फैलने वाले “अफवाहों” के प्रति हमेशा चिंतित रहना चाहिए, जबकि पुरुष अपने कामकाज पर ध्यान केंद्रित रखने और “अफवाहों” से बे-परवाह बने रहने के लिए मुक्त हैं.
आरएसएस के गुरू गोलवरकर ने महिलाओं की समानता या मुक्ति के विचारों का मखौल उड़ाया था: “आज ‘महिलाओं की समानता’ और ‘पुरुष-प्रभुत्व से उनकी मुक्ति’ का शोर मचा हुआ है! उनकी पृथक लैंगिगता के आधार पर सत्ता व शक्ति के विभिन्न संस्तरों में उनके लिए आरक्षण का दावा किया जा रहा है, और इस प्रकार जातिवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद, आदि के साथ एक और ‘वाद’ –‘लिंगवाद’ को भी जोड़ा जा रहा है.” (बंच ऑफ थाॅट्स, पृष्ठ 25).
“मुस्लिमों को स्वीकार करना”?
भागवत के इस कथन का ठीक-ठीक क्या मतलब है कि “अगर मुस्लिम नहीं शामिल होंगे, तो हिंदुत्व अधूरा रहेगा”?
उनके ही भाषण में इसका संकेत छिपा हुआ है. उन्होंने कहा, “उसको आप, हम जैसा कहते हैं उसको, हिंदू मत कहो ... आप उसको भारतीय कहो ... हम आपके कहने का सम्मान करते हैं.” तो, आरएसएस जो ‘भारत माता की जय’ कहलवाने के लिए लोगों को पीटता है, दरअसल “भारतीय” से ज्यादा “हिंदू” शब्द को तरजीह देता है; और यह सोचता है कि वह मुस्लिमों पर खुद को “भारतीय कहने देकर” उपकार कर रहा है ! बेशक भागवत भी यहां “हिंदू” और “भारतीय’ को एक समान मान रहे हैं.
बहरहाल, भागवत ने फिर यह भी कहा, “परीक्षा में जिस तरह हम पहले आसान सवालों को हल करते हैं और कठिन प्रश्नों को बाद में हाथ लगाते हैं ... (उसी तरह) पहले हम उनको संगठित करेंगे जो मानते हैं कि वे हिंदू हैं ...” इस बयान से स्पष्ट है कि वे उम्मीद करते हैं कि मुसलमान, ईसाई और अन्य अल्पसंख्यक अंततः “स्वीकार करेंगे कि वे हिंदू हैं”! यहां एक बार फिर भागवत जो कुछ कह रहे हैं वह गोलवरकर और दीन दयाल उपाध्याय के कथनों से जरा भी भिन्न नहीं है.
गोलवरकर ने 1939 में अपनी उस रचना में, जिसमें नाजी जर्मनी द्वारा यहूदियों के निष्कासन की प्रशंसा की गई है, कहा कि “... हिंदुस्तान में विदेशी नस्लों को या तो हिंदू संस्कृति और भाषा अपनानी पड़ेगी, हिंदू धर्म का सम्मान और समादर करना सीखना पड़ेगा, उन्हें हिंदू नस्ल और संस्कृति, अर्थात् हिंदू राष्ट्र के गौरवगान से इतर कोई अन्य विचार नहीं रखना होगा और उन्हें अपना पृथक अस्तित्व मिटाकर हिंदू नस्ल में विलय कर जाना होगा; अथवा वे पूरी तरह हिंदू राष्ट्र की मातहती में ही इस देश में रह सकते हैं, वे किसी चीज का दावा नहीं करेंगे, कोई तरजीही व्यवहार की बात तो दूर, उन्हें कोई विशेषाधिकार नहीं मिलेगा, यहां तक कि नागरिकों के अधिकार भी नहीं मिलेंगे.” (एमएस गोलवरकर, ‘वी ऑर आवर नेशनहुड डिफाइंड’ भारत प्रकाशन, 1939, 104-105)
गोलवरकर ने स्पष्ट कर दिया कि आरएसएस के विचार से हिंदू बहुसंख्यावादी पहचान की राजनीति ही एकमात्र स्वीकार्य राष्ट्रवाद है और हिंदू पहचान से भिन्न किसी अन्य पहचान का दावा करने की कोई भी राजनीति ‘राष्ट्र-विरोधी’ और ‘विभाजनकारी’ है. उन्होंने लिखा, “हमें याद रखना चाहिए यह एकत्व हमारे जन्म से ही हमारे रक्त में घुला-मिला है, क्योंकि हिंदुओं के रूप में ही हम सबका जन्म हुआ है.” (बंच ऑफ थाॅट्स, पृ. 255) उन्होंने ‘हिंदू मुस्लिम भाई-भाई’ के नारे पर प्रहार किया और उन्होंने आलोचना के स्वर में कहा कि “हिंदू राष्ट्रवाद की सच्ची और सकारात्मक अवधारणा को सांप्रदायिक, प्रतिक्रियावादी और संकीर्ण मानसिकता वाला विचार बताया जा रहा है.” (वही, पृ. 317)
गोलवलकर ने लिखा, “भारत में हिंदू को कभी भी ‘सांप्रदायिक’ नहीं कहा जा सकता है ... भारत के राष्ट्रीय जीवन-मूल्य वस्तुतः हिंदुओं के जीवन से निकलते हें. इस रूप में, वही यहां ‘राष्ट्रीय’ है – ‘सांप्रदायिक’ कत्तई नहीं.” (वही, पृ. 344)
तब, आरएसएस की नजर में सांप्रदायिक कौन थे ? गोलवरकर ने गैर-हिंदू पहचान रखने वाले समूहों – अर्थात मुस्लिमों और ईसाइयों – की सांप्रदायिकता समेत सात किस्म की सांप्रदायिकता की सूची बनाई. उन्होंने सिखों और नव-बौद्धों को भी सांप्रदायिक माना, क्योंकि उनके अनुसार, वे लोग पहले हिंदू समाज में शामिल थे, लेकिन बाद में वे “खुद को हिंदू समाज और धर्म से अलग समझने लगे और उस आधार पर वे अलग राजनीतिक और आर्थिक विशेषाधिकारों की मांग करने लगे ...”
इसी तरह, उन्होंने द्रविण कडगम और द्रविड़ मुनेत्र कडगम जैसी तमिल पार्टियों को भी सांप्रदायिक के बतौर चिह्नित किया, क्योंकि इन पार्टियों ने तमिल जनता और पिछड़ी जातियों की भाषाई और सांस्कृतिक विशिष्टता का दावा जताया था. सबसे गौरतलब यह है कि उन्होंने उन लोगों को भी सांप्रदायिक करार दिया “जो ‘स्पृश्यता’ और ‘अस्पृश्यता’ तथा ‘ब्राह्मण’ और ‘गैर-ब्राह्मण’ के नाम पर विवाद खड़ा करते हैं और नफरत, दुश्मनी, स्वार्थपरता फैलाते हैं, तथा विशेषाधिकार की मांग करते हैं” – यानी, दलित और पिछड़ी जातियां ! (वही, पृ. 346-47)
25 सितंबर 2016 को भाजपा की राष्ट्रीय परिषद को संबोधित करते हुए मोदी ने जन संघ के संस्थापक दीन दयाल उपाध्याय के हवाले से भाजपा कार्यकर्ताओं को उपदेश दिया कि वे “मुसलमानों को अपना सगा समझें.” इस टिप्पणी को – जो भागवत की “मुस्लिमों को स्वीकार करो” वाली टिप्पणी से इतनी मिलती-जुलती है – मीडिया ने भाजपा नेताओं की मुस्लिम विरोधी नफरत-बयानबाजी के लिए उन्हें फटकार के बतौर व्यापक रूप से प्रचारित किया. बहरहाल मोदी के असली शब्दों ने, और दीन दयाल उपाध्याय की उद्धृत रचनाओं ने, उनसे सुपरिचित श्रोताओं के बीच बिलकुल भिन्न संदेश संप्रेषित किया.
मोदी ने कहा, “पचास वर्ष पूर्व, पंडित उपाध्याय ने कहा ‘मुस्लिमों को पुरस्कृत मत करो, उन्हें तिरस्कृत मत करो, उन्हें परिष्कृत करो.’ मुसलमानों को ‘वोट की मंडी का माल’ या ‘घृणा की वस्तु’ मत समझो. ‘उन्हें अपना समझो’.
दीन दयाल को उद्धृत करने में मोदी का असली मतलब क्या था, यह दीन दयाल के लेख ‘अखंड भारत’ से स्पष्ट हो जाता है, जो 24 अगस्त 1953 को पांचजन्य में छपा था:
“... मुस्लिम समुदाय का अलगाववादी और राष्ट्र-विरोधी रवैया अखंड भारत के लिए सबसे बड़ी बाधा है ... जिन्हें अखंड भारत को लेकर संदेह है, वे महसूस करते हैं कि मुस्लिम अपनी नीति नहीं बदलेंगे. अगर ऐसा है, तो भारत में इन छह करोड़ मुसलमानों का बने रहना भारत के हितों के लिए काफी नुकसानदेह होगा. क्या कांग्रेस का कोई आदमी कहेगा कि मुसलमानों को भारत से बाहर खदेड़ देना चाहिए? अगर नहीं, तो उन्हें इस देश के राष्ट्रीय जीवन में ही समाहित कर लेना होगा. अगर भौगोलिक रूप से विभाजित भारत के अंदर (मुस्लिमों का) यह समावेशीकरण संभव है, तब शेष भू-भागों को भारत में समाहित कर लेने में ज्यादा समय नहीं लगेगा. लेकिन मुसलमानों को भारतीय बनाने के अलावा, हमें हिंदू मुस्लिम-एकता की इस 30 वर्ष पुरानी नीति को भी बदल डालना होगा, जिसे कांग्रेस ने गलत बुनियाद पर अपना रखा है. ... अगर हम एकता चाहते हैं तो हमें भारतीय राष्ट्रवाद जो हिंदू राष्ट्रवाद है, और भारतीय संस्कृति जो हिंदू संस्कृति है, का मजबूत प्रदर्शन करना होगा. हमें इसे अपने मार्ग निर्देशक उसूल के बतौर ग्रहण करना होगा.”
यहां यह स्पष्ट है कि अपने पूर्ववर्ती गोलवरकर की तरह और अपने काफी बाद मोदी और भागवत की तरह दीन दयाल उपाध्याय भारतीय राष्ट्रवाद को हिंदू राष्ट्रवाद के बराबर मान लेते हैं और वे मुस्लिमों से उम्मीद करते हैं कि वे इस हिंदू राष्ट्रवाद में समाहित हो जाएं और इसे ही अपनी पहचान बना लें. बड़ी सावधानी से भागवत ने ‘हिंदू-मुस्लिम एकता’ (जिसका मतलब है बराबरी वालों के बीच एकता) की बात नहीं कहकर हिंदुत्व में मुसलमानों को “स्वीकार करने” की बात कही. इस वक्तव्य को भागवत की इस टिप्पणी के साथ मिला कर पढ़िए कि आरएसएस “पहले उनको संगठित करेगा जो मानते हैं कि वे हिंदू हैं”, तब साफ हो जाएगा कि यह “स्वीकार करना” मुसलमानों को “समाहित करने” और उन पर “खुद को हिंदू मानने के लिए” निरंतर दबाव बनाने के हिंदुत्ववादी प्रयासों का ही एक ढंका-छुपा जुमला है.
राष्ट्रवाद के रूप में कट्टरता
भारत की अन्य राजनीतिक विचारधाराओं से अलग आरएसएस की विचारधारा औपनिवेशिक शासन के प्रतिरोध में बनी विभिन्न किस्म की जनता की एकता के बतौर भारतीय राष्ट्रवाद की परिभाषा को खारिज करती है, और राष्ट्र को इस तरह से परिभाषित करती है जिससे कि अल्पसंख्यक समुदाय के साथ-साथ सामाजिक मुक्ति और समानता के तत्व भी इसके दायरे से बहिष्कृत कर दिए जाते हैं.
1966 में ‘बंच ऑफ थाॅट्स’ में लिखते हुए गोलवरकर यह भलीभांति जानते थे कि आजादी के बाद के उस डेढ़ दशक में, बंटवारे के जख्मों के बावजूद, हिंदू-मुस्लिम एकता का विचार एक आकर्षक व लोकप्रिय विचार बना रहा था. इसीलिए, वे ‘साधारण भारतीयों’ की मुस्लिम-विरोधी कट्टरता का उदाहरण देकर यह साबित करना चाहते थे कि मुसलमान भारत के अंग नहीं हैं. गोलवरकर आरएसएस नेता बीएस मुंजे के बारे में एक कहानी बयान करते हैं, जिन्हें टिकट-कंडक्टर ने तर्क-वितर्क के दौरान भूल से मुसलमान समझ लिया था जब वे आरएसएस संस्थापक हेडगेवार के साथ यात्रा कर रहे थे. (मुंजे और हेडगेवार, दोनों मेडिकल डाॅक्टर थे और इसीलिए दोनों को ‘डाॅक्टर’ संबोधित किया गया है). “टिकट इंस्पेक्टर के अड़ियलपन को देखकर उन्होंने (मुंजे ने) गुस्से से कहा, ‘क्या तुम मेरा यकीन नहीं करते हो ? मैं रेलवे का मालिक हूं, क्योंकि मैं भाड़ा देता हूं. तुम तो एक मुलाजिम भर हो. निकल जाओ.’ टिकट इंस्पेक्टर भी गुस्सा हो गया और उसने कहा, ‘तुम कौन होते हो मुझे ऐसा कहने वाले ? यह मुस्लिम देश नहीं है, तुम निकलो यहां से.’ यह सुनकर दोनों डाॅक्टर खुल कर हंस पड़े ! उसने ऐसा क्यों कहा ? क्योंकि, डा. मुंजे की लंबी दाढ़ी थी और टिकट इंस्पेक्टर ने गलती से उन्हें मुसलमान समझ लिया. यहां तक कि एक साधारण औसत आदमी भी स्वतःस्फूर्त रूप से महसूस कर लेता है कि यह मुस्लिम देश नहीं है.” (‘बंच ऑफ थाॅट्स’, पृ. 324-25)
भागवत ने अपने सबसे हालिया बयानों में, खबरों के अनुसार, कहा है कि आरएसएस गोलवरकर के ‘बंच ऑफ थाॅट्स’ के कुछ अंशों से अलग हट रहा है, और इसकी जगह उनके “चिरस्थायी विचार” को एक “लोकप्रिय संस्करण” में प्रकाशित कर रहा है, “जिसमें तात्कालिक संदर्भों वाली तमाम टिप्पणियों को हटा कर उन टिप्पणियों को रखा जाएगा, जो युगों तक स्थायी रहने वाली हैं. आप उसमें यह (मुसलमान-दुश्मन-हैं) टिप्पणी नहीं पाएंगे”. लेकिन जैसा कि हमने देखा है, गोलवरकर की कट्टरता महज एक चलती-फिरती टिप्पणी नहीं है – यह उनकी विचारधारा और लेखों का सारतत्व है, जिसे बंच ऑफ थाॅट्स के हर पन्ने और हर पैराग्राफ में बारंबार दुहराया गया है! बंच ऑफ थाॅट्स के हर पन्ने में व्यक्त किया गया मुख्य विचार यह है कि भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं, हिंदू है और दलितों, सिखों, नव-बौद्धों और मुस्लिमों समेत वे तमाम लोग, जो खुद को हिंदू नहीं समझते हैं, और उनके साथ वे भी जो ‘हिंदू-मुस्लिम एकता’ का आह्वान करते हैं, “सांप्रदायिक” और राष्ट्र-विरोधी हैं !
आरएसएस इसके पहले भी गोलवरकर के ‘वी’ से अलग हटने का दावा कर सकता था, क्योंकि उसमें फासीवाद और यहूदी-विरोध की बेशर्म प्रशंसा की गई है. अब वे आरएसएस के दूसरे बाइबिल, बंच ऑफ थाॅट्स, को संपादित कर रहे हैं. यह बताने के बजाय कि हम आरएसएस के साहित्य की उन तमाम गलत-सलत बातों को पढ़ते रहे हैं, भागवत के लिए यह स्वीकार करना ज्यादा ईमानदारीपूर्ण नहीं होगा कि उन्हें आरएसएस की विचारधारा की पर्दादारी करनी पड़ रही है, क्योंकि अपने प्रत्यक्ष स्वरूप में यह विचारधारा व्यापक लोकतांत्रिक और प्रगतिशील भारतीयों के लिए अरुचिकर है ?
क्या भागवत यह स्वीकार करेंगे कि हेेडगेवार, गोलवरकर और मुंजे कट्टर थे और क्या भागवत उनकी भर्त्सना करेंगे? इसका जवाब है – नहीं ! इसके बजाय वे गोलवरकर को “स्वच्छ बनाने” और आरएसएस के लिए एक उदार मुखौटा निर्मित करने का प्रयास कर रहे हैं. यह फासीवाद को सम्मानजनक और स्वीकार्य बनाने – भेड़िये को भेड़ की खाल ओढ़ाने की ही एक कोशिश है.